विचार: बौद्धिक अवसाद से मुक्त हो जेएनयू
जेएनयू का मौजूदा संकट एक गहरे बौद्धिक अवसाद का लक्षण है। आंदोलनकारियों को समझना होगा कि विरोध का अधिकार देश की जनता के सामूहिक विवेक से ऊपर नहीं है। आपातकाल का कल्पित भय उन लोगों का आवरण है, जो लोकतांत्रिक संवाद का साहस खो चुके हैं।
HighLights
जेएनयू छात्र राजनीति संवैधानिक संस्थाओं को चुनौती दे रही है।
विश्वविद्यालय वैचारिक युद्धभूमि नहीं, संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करें।
करदाताओं के धन से राष्ट्र-विरोधी नारों को बढ़ावा अस्वीकार्य है।
रामानंद शर्मा। हाल में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में जो कुछ हुआ, वह केवल छात्र राजनीति की हलचल नहीं है। यह भारतीय गणराज्य के यथार्थ और परिसर की पुरानी जकड़न के बीच एक बड़ा विचलन है। साबरमती छात्रावास के पास हुई सभा जिस तरह हिंसक नारेबाजी में बदली, वह चौंकाती नहीं है। यह उस रुग्ण मानसिकता का प्रकटीकरण है, जो संवैधानिक संस्थाओं के निर्णयों को स्वीकार करने के बजाय सड़क पर चुनौती देने की आदी हो चुकी है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे ‘नफरत की प्रयोगशाला’ कहा है। दरअसल यह उस अकादमिक वामपंथ की विफलता है, जो आज भी समय की आहट नहीं सुन पा रहा। प्रखर चुनावी जनादेश के इस दौर में अब ‘दिखावे का विद्रोह’ अपनी प्रासंगिकता खो चुका है।
विश्वविद्यालय किसी विचारधारा की छावनी नहीं, बल्कि संविधान के अधीन चलने वाली सार्वजनिक संस्थाएं हैं। उनका दायित्व केवल प्रश्न उठाना नहीं, बल्कि संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर रहकर विवेक विकसित करना भी है। जब कोई परिसर स्वयं को वैचारिक युद्धभूमि में बदल लेता है, तब वह अपनी संवैधानिक पहचान खो देता है। लोकतंत्र में प्रतिरोध का स्थान है, पर वह संस्थागत संतुलन के भीतर होना चाहिए, उसके विरुद्ध नहीं। यहां नीतिगत विरोध नहीं हो रहा, बल्कि सीधे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ललकारा जा रहा है। जब छात्र राजनीति न्यायालय को भी सत्ता का औजार बताने लगती है, तब गणराज्य की अंतिम तटस्थ भूमि भी असुरक्षित हो जाती है। यह असहमति नहीं, बल्कि संवैधानिक विश्वास का क्षरण है। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र केवल टकराव का अखाड़ा बनकर रह जाता है।
उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर न्यायिक फैसला साक्ष्यों पर आधारित था, किंतु जेएनयू के एक वर्ग ने इसे ‘अन्याय’ बता दिया। उन्होंने संस्थान को अदालत के सामने खड़ा कर दिया है। जब छात्र संगठन देश के शीर्ष नेतृत्व के विरुद्ध अमर्यादित नारे लगाते हैं, तो वह वैचारिक मतभेद नहीं रहता। वह संविधान की मूल भावना का अनादर है। किसी व्यक्ति के प्रति सहानुभूति अलग बात है, पर न्यायिक प्रक्रिया को शत्रु मान लेना न्यायपालिका की अखंडता पर प्रहार है। लोकतंत्र में असहमति का स्थान न्यायालय में होता है, सड़कों पर उकसावे में नहीं। यदि छात्र राजनीति खुद को न्यायपालिका से ऊपर मान ले, तो यह गणराज्य के लिए बड़ी चिंता है।
जेएनयू जैसे संस्थान आम नागरिकों की गाढ़ी कमाई से चलते हैं। यह समाज के साथ एक नैतिक अनुबंध है। इस अनुबंध के भीतर आलोचना वैध है, पर राष्ट्र की वैधता को अपमानित करना स्वीकार्य नहीं है। करदाताओं से यह आशा करना कि वे अपनी ही बर्बादी के नारों के लिए धन दें, किसी भी समाज में संभव नहीं है। यह जवाबदेही की मांग दमन नहीं, बल्कि एक लोकतांत्रिक आवश्यकता है। शैक्षणिक स्वतंत्रता का सबसे बड़ा शत्रु प्रशासनिक नियंत्रण नहीं, बल्कि वैचारिक एकाधिकार है। जब किसी एक दृष्टिकोण को नैतिक ऊंचाई और अन्य को संदेह की दृष्टि से देखा जाए, तब परिसर स्वतः असहिष्णु हो जाता है। संस्थानों का क्षरण दमन से नहीं, विचारों की एकरूपता से होता है। विविधता पाठ्यक्रम में ही नहीं, विमर्श में भी होनी चाहिए।
कोई भी परिपक्व लोकतंत्र अपने संस्थानों को राष्ट्र के विरुद्ध भावनात्मक उभार का मंच नहीं बनने देता। परिसर की उग्र राजनीति का सबसे अनदेखा प्रभाव उन छात्रों पर पड़ता है, जो पढ़ने आए हैं, नारे लगाने नहीं। पहली पीढ़ी के विद्यार्थी, ग्रामीण पृष्ठभूमि के युवा और सीमित संसाधनों वाले छात्र सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। उनकी चुप्पी सहमति नहीं, विवशता है। विश्वविद्यालय यदि उनकी आकांक्षाओं की रक्षा नहीं करता, तो वह अपने सामाजिक दायित्व से चूक जाता है। परिसर में ‘स्थायी आंदोलन’ की प्रवृत्ति शैक्षणिक क्षरण पैदा कर रही है। जब पहचान पढ़ाई के बजाय प्रदर्शनों से होने लगे, तो छात्रों का भविष्य दांव पर लग जाता है।
दीर्घकाल में यह संस्थान को भीतर से खोखला कर देता है। वैश्विक परिदृश्य को देखिए। विकसित लोकतंत्रों ने भी अभिव्यक्ति की सीमाएं तय की हैं। फ्रांस में आतंकी समूहों के समर्थन पर गिरफ्तारियां होती हैं। अमेरिका में हिंसा भड़काने वाले भाषणों को संरक्षण नहीं मिलता। फिर भारत से ही यह अपेक्षा क्यों कि वह अपने अस्तित्व पर प्रहार करने वाली भाषा के प्रति मौन रहे? दुनिया का कोई भी उदार समाज राष्ट्र की अखंडता को खंडित करने वाले आह्वान सहन नहीं करता। भारत इस वैश्विक व्यवस्था का अपवाद नहीं हो सकता। ‘आपातकाल’ और ‘फासीवाद’ जैसे शब्दों का प्रयोग अब समाज में एक नैतिक थकान पैदा कर रहा है।
जेएनयू का मौजूदा संकट एक गहरे बौद्धिक अवसाद का लक्षण है। आंदोलनकारियों को समझना होगा कि विरोध का अधिकार देश की जनता के सामूहिक विवेक से ऊपर नहीं है। आपातकाल का कल्पित भय उन लोगों का आवरण है, जो लोकतांत्रिक संवाद का साहस खो चुके हैं। यदि जेएनयू को अपनी प्रतिष्ठा बचानी है, तो उसे कर्मकांडीय राजनीति छोड़नी होगी। उसे नफरत की प्रयोगशाला के बजाय नवाचार का केंद्र बनना होगा। अब समय आ गया है कि परिसर की राजनीति गणतांत्रिक जिम्मेदारियों को स्वीकार करे।
(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट कालेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं)









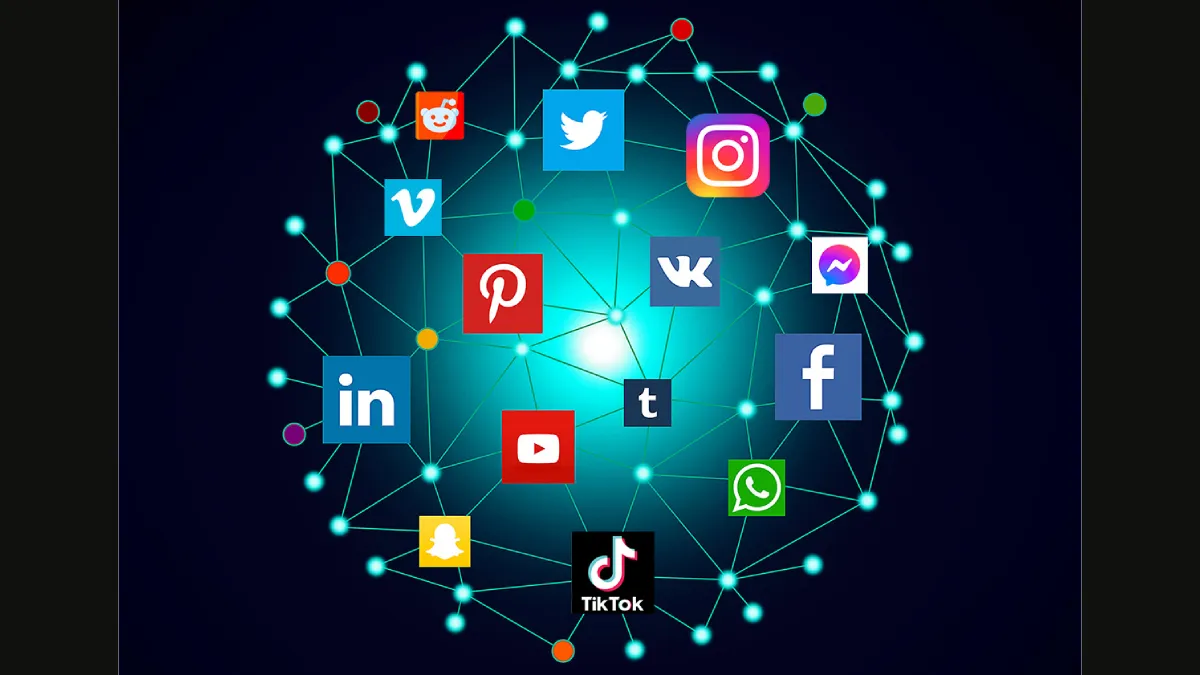



कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।